Ek Baarat Yatra : Andar Baahar (Samsmaran - A Marriage Procession)
संस्मरण
एक बारात यात्रा :
अंदर और बाहर
-हरिशंकर राढ़ी
अभी बिहार से एक
बारात करके होकर लौटा हूँ। बहुत दिनों से बिहार में किसी विवाह में सम्मिलित होने
की इच्छा थी। वैसे भी बिहार घूमने और देखने का कभी नजदीकी अवसर नहीं मिला था।
एक-दो बार ट्रेन से आना-जाना हुआ, लेकिन उसे बिहार
भ्रमण तो नहीं माना जा सकता। सुना था कि बिहार कि संस्कृति बहुत धनी है। मिथिला की
ओर विवाह एक बहुत भव्य आयोजन होता है और व्यंजनों की भरमार लग जाती है। पिछले कुछ
दशकों में बिहार कई अर्थों में बदनाम हुआ। उसकी प्रतिष्ठा में जातिवाद, बेरोजगारी, लचर कानून व्यवस्था और कुछ हद तक निम्न
जीवन स्तर ने बहुत बट्टा लगाया। बिहार की साख गिराने में पलायनवाद ने महती भूमिका
निभाई। कारण कुछ भी रहा हो, बिहार बदनाम हुआ।
फिर भी, बिहार की संस्कृति और व्यवस्था को देखने के लिए
मेरा मन कसमसाता रहा। संयोग बन गया। एक मित्र के भतीजे की षादी भागलपुर में तय हुई
तो उनका आग्रहपूर्ण आदेश आया कि बारात चलना है। उसमें भी अच्छाई यह कि दिल्ली से
एक बड़ा दल चलेगा जिसमें अधिकांश लोग मेरे नजदीकी परिचय के दायरे में। बाकी बारात
कानपुर से। अब मैं मना ही क्यों करता ?
तो
आज बारात से लौट आया। मई माह की भयंकर गर्मी के बावजूद मन शीतल हुआ। प्रस्थान से
लेकर उत्तर प्रदेश समाप्त होने तक ऐसा नहीं लगा था कि एक साथ दो बारातें चलेंगी -
एक बाहर और एक मन में। लेकिन चलीं और खूब चलीं। अंदर वाली बारात वापसी में कहीं
छूट गई या रात के अंधेरे में कहीं बिला गई। हो सकता है कि छूट ही गई हो। लेकिन
छूटा हुआ मान लेना भी ठीक नहीं क्योंकि यादें तो आई हैं। खूब झकझोरा था जाते समय
उन्होंने और पता नहीं कितना पीछे ले गई थीं। बहुत से चरित्र खयालों में आते - जाते
रहे । साथ के बाराती राजनीतिक बातों और ताश में रम रहे थे और मैं अंदर के
बारातियों से संवाद में।अमूमन
जैसा होता है, ट्रेन दो-ढाई घंटे लेट हो गई थी। मुगलसराय
(अब दीनदयाल उपाध्याय नगर) रात में निकल जाना चाहिए था, लेकिन
सुबह हो गई थी वहां पहुंचते-पहुंचते। रात में निकल गया होता तो अंदर की बारात नहीं
बनती। मुगलसराय से मेरा कोई नाता नहीं, सिवाय इसके कि एक
बड़ा जंक्शन है जिसके बारे में बचपन से सुनता आ रहा था, जब
ट्रेन को चित्र के अलावा कहीं देखा ही नहीं था। ऊपर की बर्थ से उतरकर नीचे खिड़की
के साथ बैठ चुका था। यह मालूम था कि मुगलसराय के बाद गाजीपुर जनपद आएगा और उसके
बाद हम बिहार में प्रवेश कर जाएंगे। गाजीपुर से भी मेरा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं
रहा है। पर रिष्तों का क्या, कहीं भी और कभी भी
बन जाते हैं। विक्रमशिला चलती रही और मैं पूर्वांचल की सुबह देखता रहा। खेतों की
ओर जाती गाय-भैंसें, उछलकूद करती बकरियां, षौच के लिए जाते आलसी और यत्र-तत्र बाड़ से घिरी जा़यद की फसलें।
गाड़ी
की गति थोड़ी थमी। जमनियाँ। पहला स्टेशन जिसने मेरे मन-मस्तिश्क पर दस्तक दी।
जमनियाँ से मेरा कोई निजी परिचय नहीं, कोई रिश्ता नहीं पर
समाया है बहुत गहरे तक। इसे मैं अपनी साहित्यिक अभिरुचि का पहला पड़ाव मानता हूँ।
बी.ए. के दिनों में डॉ. शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास ‘अलग-अलग
बैतरणी’ हाथ लग गया था। परीक्षा के बाद समयकर्तन की इच्छा
से कुछ पठनीय ढूंढ रहा था कि इससे सामना हो गया। बिलकुल पुराना संस्करण, मोटा आकार। इतना अधिक पढ़ने का साहस तो नहीं था, लेकिन
शुरू हो गया। यहीं से जमनियाँ ये परिचय हुआ और फिर प्रगाढ़ता।
एक
स्थान के रूप में जमनियाँ ‘अलग-अलग बैतरणी’
के केंद्र में है। शिवप्रसाद सिंह ने इसके कथानक में ग्रामीण जीवन के न
जाने कितने रंग और कितने मिथक पिरोये हैं। जमनियाँ की गोद में समाया ‘नाचिरागी मौजा’ करैता पूरे बिहार
और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। स्वातंत्र्योत्तर उत्तर भारत के
गांवों में बदलते परिवेश, टूटते मिथकों,
दरकते रिश्तों तथा विखंडित होती परंपराओं का शब्दचित्र है यह उपन्यास।
ग्रामीण परिवेश में घुसती स्वार्थी राजनीति, सामंतवाद
की टूटन, उसे बचाए रखने की जद्दोजहद, विषैले
होते ताल्लुकात, उन्हीं में संकोच तले विकसित होते प्रेम
संबंध और खांटी ग्रामीण मानसिकता का जो निरूपण ‘अलग-अलग
बैतरणी’ में मिलता है, वह
अन्यत्र दुर्लभ है। सच तो यह है कि यह पचास से लेकर अस्सी के दशक तक के गांवों की
डाक्यूमेंट्री है। शायद ही किसी प्रकार का ग्रामीण चरित्र होगा जो इस कथा का
हिस्सा बनने से रह गया होगा। जमींदार जैपाल सिंह, बुझारथ,
बीसू धोबी, दयाल महराज, सुरजू
सिंह, विपिन, पुष्पा, कनिया, पटनहिया भाभी, जग्गन
मिसिर, डॉ. देवकांत, मास्टर
शशिकांत, खलील मियाँ और न जाने कितने जीवंत चरित्र पाठक के
मन में स्थायी निवास बना लेते हैं। न जाने कितने प्रसंगों में डॉ. देवकांत,
विपिन, जग्गन मिसिर और मास्टर षशिकांत के माध्यम
से गांव की स्थिति पर सार्थक, सटीक और गंभीर
विमर्श चलाया है उपन्यासकार ने। कोई भी तबका लेखक की नज़रों से बच नहीं पाया है।
बहुत
दिनों तक गूँजता रहा था यह उपन्यास मेरे अंदर। उसका हर पात्र मुझे अपने गांव में
दिखाई देता था। विशेषतः जग्गन मिसिर, बुझारथ, सुरजू सिंह तो साक्षात घूमते हुए दिखाई देते थे। करैता से पलायन करने
वाला हर चरित्र जमनियाँ होकर ही जाता है। बाद में पता चला कि शिवप्रसाद सिंह की
माध्यमिक शिक्षा जमनियाँ में हुई थी। उस क्षेत्र को उन्होंने जिया था और उसे ही
ज्यों का त्यों उतार दिया था ‘अलग-अलग बैतरणी’
में।
बाद
में उनके लिखे दो और उपन्यास पढ़ने को मिले - ‘गली
आगे मुड़ती’ है तथा ‘औरत’। लेकिन मन में चढ़ा था तो केवल ‘अलग-अलग बैतरणी’
ही। गोरखपुर में अंगरेजी में एम. ए. करते समय मैंने उन्हें एक पत्र भी
लिखा था जिसका जवाब लौटती डाक से आया था। एक दो पत्र और आए होंगे लेकिन वे कहां खो
गए, याद नहीं। तब नहीं मालूम था कि अक्षरों की दुनिया
में अपना प्रवेश भी होगा, भले ही एक अकिंचन
के रूप में !
तो
जमनियाँ स्टेशन आया और चला गया। अंदर ही अंदर ‘अलग-अलग
बैतरणी’ की यात्रा चलती रही। इतने में भदौरा स्टेशन आ गया।
एक पल को कुछ झटका सा लगा। क्या मैं भदौरा को भी जानता हूँ ? कहाँ और कब देखा ? याद आया - शायद
यहीं के अपने अग्रज मित्र, आत्मीय नवगीतकार ओम
धीरज जी हैं। वे गाजीपुर के ही हैं। गाजीपुर, बनारस
और आजमगढ़ में बहुत सारे साम्य हैं। भाषा, संस्कृति, खान-पान और व्यवहार में शायद ही कोई अंतर हो इन जिलों में। हाँ, वे इसी इलाके के हैं। ओम धीरज जी के तीनों नवगीत संग्रहों - बेघर हुए
अलाव, सावन सूखे पाँव और बँधे नाव किस ठाँव से मैं ठीक
से गुज़र चुका हूँ। इन पर समीक्षा भी लिखी है मैंने। ओम धीरज के नवगीत यहां की
मिट्टी, मिठास और मूल्यों को लेकर चलते हैं। एक में कहा
जाए तो पकी इमली सा स्वाद होता है इनका। कभी-कभी लगता है कि ओम धीरज जी ने स्व0 शिवप्रसाद सिंह की आंचलिक गद्य परंपरा निहायत खूबसूरती और सामासिकता से
अपने नवगीतों में ढाल लिया है। पूरा एक कालखंड और भौगोलिक अंचल बोलता है धीरज जी
के नवगीतों में। नवगीतों की दुनिया में ओम धीरज जी निश्चित रूप से एक सशक्त
हस्ताक्षर हैं। रही-सही कसर उनका स्वभाव और व्यक्तिगत मित्रता पूरी कर देती है।
ट्रेन तो नहीं रुकी भदौरा में, लेकिन मन रुका रहा
और देखता रहा उनके नवगीतों को।
अब
गहमर आ गए थे हम। गहमर से भी मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। लगाव गहमर से नहीं,
गहमरी से है। भोजपुरी के बड़े आत्मीय कवि स्वर्गीय भोलानाथ गहमरी।
उन्होंने गहमर को खुद से बड़ा मानकर अपने नाम के साथ जोड़ा लेकिन बड़ा हो गया गहमरी।
बड़ा सुखद लगता है मुझे कि अपने देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जो किसी कवि या लेखक के
नाम से जुड़कर प्रसिद्ध हुई हैं। मैं भोलानाथ गहमरी को व्यक्तिगत रूप से नहीं
जानता। शायद जान भी नहीं सकता था।
सत्तर
और अस्सी का दशक आकाशवाणी युग था। रेडियो मनोरंजन का सबसे बड़ा और उपयोगी साधन था,
हालांकि यह भी सर्वसुलभ नहीं था। उन दिनों पूर्वी उत्तरप्रदेश और भोजपुरी
भाशी बिहार के सभी आकाशवाणी केंद्रों से मोहम्मद खलील के लोकगीत गूँजा करते थे।
षाम होते ही खेती-बारी, कृशि जगत या गाँव की ओर जैसे कार्यक्रम
शुरू हो जाते। इनमें कृषि विकास की तकनीक सिखाई जाती थी। स्वयं समर्थ बनने के लिए
कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर था। कार्यक्रम के बीच में एक लोकगीत जरूर प्रस्तुत किया
जाता था।
पिताजी
आकाशवाणी का गोरखपुर या वाराणसी केंद्र समयानुसार लगाकर बैठ जाते। खेती के बारे
में उतनी रुचि नहीं रहती थी जितनी एक भोजपुरी लोकगीत सुनने की अभिलाषा। ऐसे में
किसी दिन जब मोहम्मद खलील का गीत बज जाता तो जैसे सबकुछ सार्थक हो जाता। गीत होते
समय किसी का बोलना पूरी तरह निषिद्ध होता। सारा वातावरण जैसे झूम उठता और रस की
बरसात होने लगती। ‘कवने खोंतवा में लुकइलू अहि रे बालम चिरई’,
‘छलकल गगरिया मोर निरमोहिया’ या फिर ‘अंगुरी में डँसले बिया नगिनिया हो ये ननदो दियना जराइ दा’ उस समय के सुपरहिट गीत थे। मैं भी इन गीतों का दीवाना था। मोहम्मद खलील
की आवाज और गायकी में एक जादू था, एक तिलिस्म था और
एक सूफियाना अंदाज। वे मेरी किशोरावस्था या नवयौवनावस्था के दिन थे। हमारे लिए
मुख्यतः गायक ही महत्त्वपूर्ण होता था, कवि या गीतकार
नहीं। कुछ दिनों बाद जानकारी हुई थी कि ‘कवने खोंतवा में
लुकइलू’ तथा ‘ले ले अइहा बालम
बजरिया से चुनरी’ के गीतकार गाजीपुर, गहमर
के कवि-गीतकार भोलानाथ गहमरी थे। ऐसे न जाने कितने गीत गहमरी ने लिखे। उनके गीतों
में भोजपुरी आत्मा बसती थी, संवेदनाएं फड़कती
थीं और भाव सीधे दिल से जुड़ जाते थे। लेकिन यदि उन्हें मोहम्मद खलील का स्वर नहीं
मिलता तो शायद वे खंडहर के गुलाब ही रह जाते। अपना स्वर देकर खलील ने उन गीतों को
अमर कर दिया। ये गहमर उन्हीं गहमरी की थाती है, मुझे
तो जुड़ना ही है। हाँ, दुख भी हुआ। मेरे साथ तमाम बुद्धिजीवी और
उच्चशिक्षित लोग थे, लेकिन शायद ही कोई गहमरी से जुड़ा हो। बस
चर्चा राजनीति की या फिर मशगूलियत ताश के पत्तों में।
खंडहर
के गुलाब तो मोहम्मद खलील भी रह गए। पूर्वांचल के न जाने कितने गीतकारों को
उन्होंने स्वर दिया या होठों से छूकर गीतों को अमर कर दिया। छपरा के पं. महेंदर
मिसिर हों या बलिया के पं. सीताराम द्विवेदी, उनके
गीतों को विस्तार दिया मोहम्मद खलील ने ही। महेंदर मिसिर के गीत मार्मिकता की हद
तक मार करते थे। वे जनकवि थे और लोगों के दिल तक पहुंचते थे। ‘अंगुरी में डंसले बिया नगिनिया हो’ ने
महेंदर मिसिर को बड़ी प्रसिद्धि दिलाई। जब मोहम्मद खलील इस गीत को गाते तो सन्नाटा
पसर जाता, लगता जैसे नागिन सबके कलेजों पर लोट रही हो। इस
दर्द में गिरमिटया हो जाने जैसा दर्द और घातक प्रहार करता। वैसे भी महेंदर मिसिर
के गीत जनपीड़ा से जुडे हुए थे। उन दिनों उनका एक गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था -
टुटही मड़इया महलिया से पूछे, घास झुलसानी
हरियलिया से पूछे, का हमरो दिनवाँ बहुरिहैं की नाहीं। मेरी
जानकारी के अनुसार इस गीत को मोहम्मद खलील ने नहीं गाया था। ‘कवनो जतन बता के जइहा, कइसे दिन बीती राम’
को किंचित परिवर्तन के साथ शारदा सिन्हा ने गाया था। इसके अलावा यह गीत
उधर की नौटंकी और नाच कार्यक्रमों में बहुत लोकप्रिय हुआ था। महेंदर मिसिर के
गीतों का जमाना भोजपुरी की बढ़ती अश्लीलता में कहीं बह गया।
मोहम्मद
खलील भोजपुरी गायक ही नहीं थे, वे भोजपुरी
संस्कृति और परंपरा थे। उन्होंने एक भी अश्लील गीत नहीं गाया। पं. सीताराम
द्विवेदी का लिखा गीत ‘छलकल गगरिया मोर निरमोहिया’ मील का पत्थर साबित हुआ था। जब भी मोहम्मद खलील के स्वर में यह गीत बजता
तो सब कुछ स्थिर हो जाता। मोहम्मद खलील धर्म - संप्रदाय से ऊपर थे। उनके स्वर में
भोजपुरी आत्मा बसती थी। उनका गाया ‘सुमिरीला शारदा
भवानी, पत राखीं महरानी’ भोजपुरी
क्षेत्र की लोकप्रिय सरस्वती वंदना थी जो अनेक अवसरों पर गाई जाती थी। रेलवे में
साधारण से पद पर कार्यरत मोहम्मद खलील मधुमेह के चलते असमय कालग्रस्त हो गए। उनके
गीतों के कैसेट या सीडी बाजार में लाए ही नहीं गए। एक-दो बार मैंने भी आकाशवाणी
गोरखपुर से प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। न अब वे गीत सुनने वाले रहे और न
गाने वाले। अश्लीलता के इस युग में मोहम्मद खलील, महेंदर
मिसिर या भोलानाथ गहमरी किस बूते टिकते ? पच्चीस-तीस की उम्र
तक पहुँचती नई पीढ़ी तो इनके नाम से भी परिचित नहीं। लेकिन इधर सुखद ये रहा कि आखर
भोजपुरी नामक किसी संस्था ने इन गीतों कहीं से प्राप्त करके यू ट्यूब पर अपलोड
किया है। वही आवाज, वही साज। बहुत अच्छा लगा। पुरबिया तान नामक
किसी संस्था ने चंदन तिवारी से इनके कई गीत ढंग से गवाए हैं। कभी-कभी उम्मीद जागती
है कि चंदन तिवारी और मैथिली ठाकुर जैसी नवोदित गायिकाएं इस परंपरा को जीवित
रखेंगी।
विचारों
तथा यादों की शृंखला भागती हुई कर्मनाशा तक आ गई। कर्मनाशा भी मेरी यादों के
तहखाने में कैद है। इसलिए नहीं कि यह एक पौराणिक नदी है और त्रिशंकु की लार से
निकली है। इसलिए भी नहीं कि इसमें नहाने से समस्त अर्जित पुण्य नष्ट हो जाता है और
इसलिए भी नहीं कि जब इसमें बाढ़ आती है तो यह मानुश बलि लेकर ही जाती है। मेरी
यादों में यह एक बार पुनः शिवप्रसाद सिंह की कहानी ‘कर्मनाशा
की हार’ के कारण बसी है। इस कहानी का पभाव इतना अधिक पड़ा
था कि मुझे कर्मनाशा सदैव हारी हुई ही दिखी है। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में इस
कहानी को पढ़ने का मौका मिला था। अंधविश्वास, जातीय
भेद और तुगलकी फरमान को जिस तरह यह कहानी तोड़ती है, उसमें
कर्मनाशा की हार होनी ही है।
कर्मनाशा
उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। नदी के पश्चिम उत्तर प्रदेश का
गाजीपुर जिला है और पूरब में बिहार का आरा। गाजियाबाद से गाजीपुर तक फैले उत्तर
प्रदेश को कर्मनाशा अलग करती है। चौड़ाई तो अधिक नहीं है, किंतु
गहराई है जिससे नदी डरावनी लगती है। न जाने वह कौन सा मिथक या मानसिकता है जो एक
नदी को पुण्यनाशिनी का विशेशण दे देता है। कर्मनाशा का उल्लेख रामचरित मानस में कई
बार आता है और प्रायः नकारात्मक अर्थ में ही आता है। लेकिन अयोध्याकांड में
तुलसीदास लिखते हैं - करमनास जल सुरसरि परई, कहहु
तासु को सीस न धरई। अर्थात कर्मनाशा का जल (जो पापदायक है) गंगा में मिलने के बाद
षीश पर धारण करने योग्य हो जाता है। समझ में नहीं आता कि जो नदी इतने लोगों को
जीवन देने का कार्य करती है, वह कर्मनाशा कैसे
हो सकती है?
क्रमशः
बक्सर और डुमराँव आते हैं। डुमराँव उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ से जुडा़ है। आगे जाता
हूँ तो आरा जिला आता है। वैसे तो आरा एक भोजपुरी फिल्मी गाने में नायिका की कमर के
साथ हिलता हुआ दिखाया गया है जिसके साथ छपरा जिला भी हिलता है। लेकिन मेरा इससे
कुछ लेना-देना नहीं है। मेरे अग्रजवत मित्र और यशस्वी संगीतज्ञ पं0 विजयशंकर मिश्र जी यहां आया करते हैं और प्रायः जिक्र भी किया करते हैं।
आरा से उनका विशेष लगाव है। आरा एक ऐतिहासिक जिला है। यह वीर कुँवर सिंह का
कर्मक्षेत्र है जहां उन्होंने अंगरेजों को मात दी थी, भले
ही कुछ समय के लिए।
अब
दानापुर आता है। दानापुर मेरी यादों का एक सुखद प्रेत है। न तो मैं कभी यहां आया
हूँ और न इससे मेरा प्रत्यक्ष संबंध है। बस कुछ यादें जुड़ी हैं पिताजी के कारण।
उन्हीं से मैंने यह नाम सुना था। तब मैं दस वर्श से अधिक का नहीं रहा होऊँगा। शायद
कम ही। सत्तर का दशक था वह। अपने जिला मुख्यालय आजमगढ़ का भी मुँह नहीं देखा था
मैंने। अभावों के दिन थे। हिस्से में यदि आवश्यकता से अधिक कुछ था तो माता-पिताजी,
बड़ी बहन ‘दीदी’ एवं
बड़े भाई ‘भइया’ का प्यार। अभावों
का हमला मेरे ऊपर सबसे बाद में होता था, या प्रायः नहीं भी
हो पाता था। मेरी बड़ी बुआ कलकत्ता रहती थीं। उनका हमें बहुत घमंड रहता था, पता नहीं क्यां। शायद समृद्ध थीं, इसलिए।
उनके बड़े बेटे पटना में किसी अच्छे पद पर थे। बुआजी शायद पटना आई हुई थीं और
उन्होंने पत्र लिखकर पिताजी को बुलाया था। क्यों, ये
मालूम नहीं। पिताजी अब होते तो जरूर पूछता और पूरी कहानी पूछता। वे किस्सागोई में
बहुत माहिर थे। सो, पिताजी पटना गए थे। वादा था कि तीन-चार
दिन में लौट आएंगे। हफ्ते के आस - पास निकल गए और वे नहीं आए। मैं हर शाम उनकी राह
देखता। मैं ही क्यों, पूरा परिवार देखता। कुल पांच जने का
परिवार एक बड़ी सी बखरी में रहता जिसकी संभाल भी मुश्किल हो रही थी। गाँव के बाहर
घर था। शाम होते ही सियारों की हुआँ-हुआँ षुरू हो जाती। यदि रात अंधेरी हो तो
चोरां का आतंक ऊपर से। ऐसे में घर में अकेली माँ और अधिकतम पंद्रह साल तक के
बच्चे।
उदासी
बढ़ने लगी थी। न तो फोन का जमाना और न संदेश की सुविधा। पता नहीं क्या हुआ पिताजी
को ! भइया-दीदी तो कम पूछते, मैं बहुत पूछता
उनके बारे में। कब आएंगे बबुआ ? क्यों नहीं आ रहे
हैं ? और अम्मा का वही धीरज भरा जवाब कि आ जाएंगे। हफ्ता
बीतते-बीतते बहुत सी आशंकाएँ घिर आई थीं। मेरा कलेजा मुँह को आ जाता। अपने छोटे से
दिल से भगवान को बहुत मनाता कि बबुआ वापस आ जाएँ। माँ दिलासे के लिए कहतीं कि बहुत
सामान लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, तो मुझे बहुत बुरा
लगता। कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन तब मैं शायद ही समझता रहा होऊँगा कि मुझसे
ज्यादा दुखी और परेशान तो अम्मा ही होंगी।
पिताजी
उस दिन शाम को आए थे। राह देखना सफल हुआ था मेरा। घर के पिछवाड़े थे तभी दौड़कर चिपट
गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि उनका लाया कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। अच्छा
लगा था तो बस उनका वापस आना। रात में उन्होंने अपनी शैली में यात्रा संस्मरण
सुनाया था। यह कि बुआ जी ने जबरदस्ती रोक लिया था। यह भी नहीं सोचा था कि बच्चों
पर क्या बीत रही होगी। वह जमाना जबरदस्ती रोके जाने का था। और हाँ, पिताजी दानापुर में किसी संकट में फंस गए थे। मुश्किल से जान बची थी। अब
याद नहीं, शायद चोरों-ठगों का गिरोह पीछे लग गया था। तबसे
दानापुर यादों में बसा रहा है। दानापुर पिताजी की याद ताजा करा गया। न जाने किस
जगह वे संकट में फंसे थे, कैसे फंसे थे,
इसका नाट्य रूपांतरण मन ही मन होने लगा था।
भागलपुर
तक पहुंचने में विक्रमशिला ने पौन तीन बजा दिए थे। वहाँ से उतरकर हम नाथ नगर गए
जहां जनवासे की व्यवस्था थी। व्यवस्था अच्छी थी, अच्छा
लगा।
 |
| प्रेम प्रभाकर जी एवं भाभी जी के साथ मैं |
भागलपुर
जाने के पीछे केवल मित्र का आग्रह, बिहार की
संस्कृति-परंपरा एवं विवाह देखना ही नहीं था। भागलपुर से एक गहरा लगाव वरिश्ठ
साहित्यकार, आलोचक, अध्येता
और भागलपुर विष्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर साहित्यिक मित्र प्रेम
प्रभाकर जी के कारण भी है। हम लोगों के संपर्क में आए लंबा अरसा नहीं हुआ है,
लेकिन वैचारिक सहमति एवं साहित्य ने बहुत नजदीक कर दिया है। भागलपुर जाने
के पीछे यह आकर्षण कम नहीं था।
शाम
को प्रेम प्रभाकर जी ने मुझे लेने के लिए अपने एक शोधछात्र प्रकाश जी को भेज दिया
था। प्रकाश बड़े आज्ञाकारी एवं सरल छात्र हैं। प्रभाकर जी के घर जाकर मुझे लगा ही
नहीं कि इनके यहां मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं जिस सरलता की तलाश में रहता हूँ,
वह प्रभाकर जी के यहां साकार रूप में बैठी है। बहुत देर तक साहित्यिक एवं
पारिवारिक चर्चा होती रही। साथ में भाभी जी (श्रीमती प्रभाकर जी) भी चर्चा में भाग
लेती रहीं। आना जरूरी था, आखिर बाराती बनकर
गया था। शादी में भी भागीदारी कैसे न निभाता ? चलते
समय प्रेम प्रभाकर जी ने अपनी आलोचनात्मक पुस्तक ‘हिंदी
कहानी का नवाँ दशक और कृषक’ की प्रति भेंट की।
यह अपने विषय की अनूठी पुस्तक है। इस विषय पर शायद ही शोध हुआ होगा। पुस्तक प्रथम
दृष्टि में ही एक सार्थक प्रयास लगती है। मिलना तो और भी साहित्यकारों से था,
ऐसा आग्रह भी था, लेकिन समय को कौन
रोक पाया है।
शादी में शामिल होकर अगली दोपहर दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। वापसी में कुछ भी विशेष नहीं रहा। एकाध घटना जरूर ऐसी हुई कि जिक्र करना अच्छा रहेगा , लेकिन जिक्र न करना उससे भी अच्छा।
(जून 01,
2019)






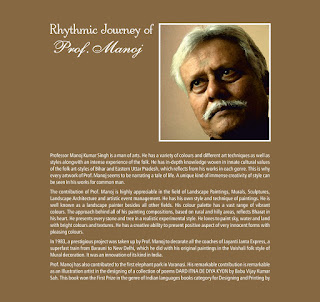


Comments
Post a Comment
सुस्वागतम!!