हिंदी सिनेमा और सब आपका
हर हफ्ते 10-20 ठो फिल्में रिलीज होती हैं. उनमें एकाध बड़े बजट की होती हैं. महीने-दो महीने में एक-दो बहुतै बड़े बजट वाली फिल्में भी आती हैं.
अब ये इतना बड़ा वाला बजट आता कहाँ से है और इससे जो वसूली होती है, उसका रिटर्न जाता कहाँ तक और कैसे है, ये जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जो नहीं जानते वो तो यह भी नहीं जानते कि परदे का हीरो वास्तव में कितना साहसी और दिलदार होता है, यह भी कि हो सकता है कि परदे का विलेन वाकई कोई नेक इंसान हो पर हीरो से ये उम्मीद बेमानी है. करीब-करीब उतनी ही बेमानी जितनी हिंदी के किसी नामी साहित्यकार के साहित्य में सच की अपेक्षा.
तो बात बड़े बजट वाली फिल्मों की हो रही थी. ये जो बड़े बजट वाली फिल्में होती हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उस बड़े बजट की वसूली होती है. दर्शक आमतौर पर सिनेमाहाल तक जाना नहीं चाहता. वैसे भारत में सिनेमाहाल तक जाने वाले आम तौर पर तीन ही तरह के लोग होते रहे हैं. या तो वे जो परम फालतू किस्म के लोग हैं. जिनमें थोड़े-बहुत मामूली अंतर के साथ वही कहानी बार-बार झेलने की हिम्मत है. या फिर वे जिनका पृथ्वी नामक ग्रह पर अवतार ही पंखा बनने के लिए हुआ है.
अगर उन्हें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, मोदीजी, राहुलजी, गांधीवाद, साम्यवाद या कोई और जी या वाद नहीं मिलेंगे तो वे छिपकलीजी, केंचुआजी, साँपजी, बिच्छूजी आदि किसी के भी पंखे हो जाएंगे और उनके लिए कुछ न कुछ देखने-सुनने या करने जाएंगे. वास्तव में ये लोग परोपकारी हैं और इन्हीं के भरोसे संसार चल रहा है. अगर ये न हों ये जो पृथ्वी नाम का ग्रह सूर्य नाम के गैसीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगाना बंद कर दे और दुनिया एक जगह ठहर जाए. तीसरी कटेगरी के दर्शक वे लोग हैं जिन्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं. सिनेमा से भी नहीं. मने परमसंत कटेगरी वाले. इन्हें सिर्फ़ तीन घंटे का मनोरंजन चाहिए होता है और मनोरंजन का मतलब इनके लिए बस मारधाड़, देहदर्शन, नाच-गाने तक सीमित है. इससे ज्यादा कुछ नहीं.
इन तीन वर्गों को भी अब हॉल तक जाने की जरूरत महसूस नहीं होती. क्योंकि नेट 400 रुपये में तीन महीने के लिए उपलब्ध है और लगभग हर हाथ में अच्छा-बुरा किसी न किसी तरह का स्मार्टफोन है. लेकिन फिल्में बनाने वालों का पैसा वसूल तो दर्शक को हॉल में ढटिया कर ही होना है. तो इसके लिए उसे मजबूर किया जाता है. डंडे से हाँक-हाँककर हॉल तक लाया और फिर दो-तीन घंटे के लिए ढटियाया जाता है.
यह डंडा अदृश्य किस्म का होता है. बिना मुद्दे के मुद्दे यानी किसी न किसी कृत्रिम मुद्दे पर बनने वाली फिल्मों पर कृत्रिम विवाद उठाया जाता है. यह कृत्रिम विवाद उठाने के लिए शुरू में कुछ लोगों को पैसा दिया जाता है. बाद में लोग इसमें लोग अपने-आप ही शामिल होते चले जाते हैं. चूँकि देश आजकल राजनीतिक रूप से दो कटेगरी में बँटा हुआ है और दोनों कटेगरियां अपनी पीढ़ियों की वास्तविक दोस्ती तक भुला कर नई-नई बनी छद्म राजनीतिक दुश्मनी निभा रही हैं, तो किसी विवाद में शामिल करने के लिए लोग ढूँढने भी नहीं पड़ते. अधिकतर तो पहले से ही मुफ्त का बेल्ट लगाकर बैठे होते हैं.
याद करिए वो फिल्म जिस पर पूरा राजस्थान धधक उठा था. बाद में रिलीज होने पर इस हाथी के दिल को चीरा तो पता चला कि इक कतर-ए-खूँ भी न निकला. उसके बाद उसी राजपूती आन-बान को बट्टा लगाने वाली बहुत बातें असली दुनिया में हुईं. उसी राजस्थान में ही. लेकिन कुछ हुआ क्या? फिर पता चला क्या किसी सेना का? फिर ये सेना एक टुच्ची फिल्म के लिए कहाँ से टपक पड़ी थी?
ये तो बस हाल का एक विवाद है. ऐसे कम से कम एक हज़ार विवाद भारत में हो चुके हैं. क्या इनसे कभी कोई हल निकला है. आजकल फिर ऐसे ही कुछ प्यालियों में तूफान उठाए जाने की कोशिश की जा रही है. धीरे-धीरे टेम्पो बन भी रहा है और फिर उफन कर बैठ भी जा रहा है. लेकिन होगा क्या? फिर वही ढाक के तीन पात. क्योंकि पहले भी मुद्दे और विवाद दोनों कृत्रिम थे और आज भी स्थिति वही है.
आप याद करिए, सीधे आपके असली मुद्दे को केंद्र में रखकर कोई सच्ची फिल्म बनी हो? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो तीन घंटे में पोएटिक जस्टिस थमा के आपको हॉल से बाहर कर देती हैं. तीन मिनट में साहूकार खेत को हड़पता है और पाँचवें मिनट में शेखचिल्ली टाइप हीरो उसके सारे गुंडों को मारकर गाँव वालों को जिता देता है. किसी राज्य के मुख्यमंत्री को एक दरोगा लतियाते हुए लॉकअप में बंद कर देता है. देखते-देखते फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है और उसके तुरंत बाद पूँजीपति मान जाता है. हम सब जानते हैं कि यह सब सिर्फ हिंदी सिनेमा में होता है, बाकी किसी सिनेमा में भी नहीं. और वास्तविक जीवन से तो इसका उतना भी संबंध नहीं है जितना बुद्धिजीवियों का सच्चाई से होता है.
याद करिए, इतने दिनों में एक भी फिल्म बनी हो भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्या को जमीनी तौर पर संबोधित करती हो? एक भी फिल्म बनी हो जो भारत में शिक्षा-व्यवस्था की बुनियादी समस्याओं को संबोधित करती हो? रोजगार की ही बात उठा लीजिए. अच्छा आइए, इतिहास की ही बात उठा लेते हैं. बाजीराव जैसे योद्धा को हिंदी सिनेमा देवदास बना के धर देता है. विभाजन के नाम पर केवल झूठ का प्रदर्शन है. सौ प्रतिशत शुद्ध झूठ. लिखित और सर्वस्वीकृत ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत. वह भी तब जबकि फिल्में बनाने वाले कुछ बड़े घराने खुद विभाजन के शिकार रहे हैंं. जिस समय विभाजन हुआ, केवल पंजाब ही नहीं बँटा था, बंगाल का सेना चीरा गया था. बंगाल के विभाजन का दर्द कहीं दिखाई देता है क्या? या विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बंग्लादेश) से जो लोग भगाए गए, वे बड़े मजे-मजे में चले आए?
दलित बड़ा प्रिय विषय है हमारे बुद्धिजीवियों का और सिनेमा में बुद्धिजीवी होने के भ्रम के शिकार कम लोग नहीं हैं. मने सब जगह हो सकते हैं बुद्धिजीवी तो सिनेमा में क्यों नहीं? तो दलितों पर उन्होंने खूब बनाया. लेकिन बनाया क्या? उसके दुख की पैरोडी, मजाक. भारत-विभाजन के समय एक जोगेंद्र नाथ मंडल हुआ करते थे. डॉ. अंबेडकर के बाद दूसरे बड़े दलित नेता. दोनों में फर्क यह था कि अंबेडकर वाकई दलित हितैषी थे और सच्चे अर्थों में मनुष्यतावादी भी, मंडलजी के लिए दलित अपने राजनीतिक स्वार्थसाधन का एक उपयोगी सामान मात्र था. तो मंडल जी अपने समय के पाकिस्तान में मंत्री बना दिए गए थे. उन्होंने पाकिस्तान बनवाने के लिए भी दलितों का कुछ इस्तेमाल किया और डॉ. अंबेडकर के मना करने के बावजूद बड़ी मात्रा में दलितों को पाकिस्तान में थोड़े दिन रोका. बाद में जब उन पर इस्लामी कहर बरपना शुरू हुआ तो मंडल जी रह पाए और न दलित. मंडल जी तो खैर बड़े आदमी थे, भाग आए. लेकिन जो आम दलित वहाँ रह गए थे, वे? उनकी सुहि लेने की जहमत न साहित्य ने उठाई और न सिनेमा ने.
सिनेमा की मानें तो थाने में कहीं घूस नहीं चलता. दरोगा जी संसार के सबसे ईमानदार प्राणी हैं. कानून अंधा है, लेकिन जज साहब भगवान से भी सच्चे हैं. झुग्गियाँ उजाड़ी जाती हैं. उजाड़ने वाले पूँजीपति के गुंडे होते हैं. लेकिन झुग्गियां बसाने के लिए हर साल इंसानों की ये जो बाढ़ आती है, ये आती कहाँ से है? यह सब पोएटिक जस्टिस का सतही तौर निपटे जा सकते लायक विषय नहीं हैं. ये और ऐसे ही और कई विषय हमारे सामाजिक जीवन के जटिल यथार्थ हैं. इनमें मसाला नहीं है. कड़वाहट है और जटिलताएँ हैं. और जहाँ यह सब है, वहाँ कम से कम हिंदी सिनेमा तो नहीं जाता.
फिर भी आप हॉल तक जाना चाहते हैं तो जरूर जाएँ. आख़िर जेब आपकी है, समय आपका, मन आपका और ईश्वर की कृपा से झेलने की कूवत भी आपकी ही.
अब ये इतना बड़ा वाला बजट आता कहाँ से है और इससे जो वसूली होती है, उसका रिटर्न जाता कहाँ तक और कैसे है, ये जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जो नहीं जानते वो तो यह भी नहीं जानते कि परदे का हीरो वास्तव में कितना साहसी और दिलदार होता है, यह भी कि हो सकता है कि परदे का विलेन वाकई कोई नेक इंसान हो पर हीरो से ये उम्मीद बेमानी है. करीब-करीब उतनी ही बेमानी जितनी हिंदी के किसी नामी साहित्यकार के साहित्य में सच की अपेक्षा.
तो बात बड़े बजट वाली फिल्मों की हो रही थी. ये जो बड़े बजट वाली फिल्में होती हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उस बड़े बजट की वसूली होती है. दर्शक आमतौर पर सिनेमाहाल तक जाना नहीं चाहता. वैसे भारत में सिनेमाहाल तक जाने वाले आम तौर पर तीन ही तरह के लोग होते रहे हैं. या तो वे जो परम फालतू किस्म के लोग हैं. जिनमें थोड़े-बहुत मामूली अंतर के साथ वही कहानी बार-बार झेलने की हिम्मत है. या फिर वे जिनका पृथ्वी नामक ग्रह पर अवतार ही पंखा बनने के लिए हुआ है.
अगर उन्हें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, मोदीजी, राहुलजी, गांधीवाद, साम्यवाद या कोई और जी या वाद नहीं मिलेंगे तो वे छिपकलीजी, केंचुआजी, साँपजी, बिच्छूजी आदि किसी के भी पंखे हो जाएंगे और उनके लिए कुछ न कुछ देखने-सुनने या करने जाएंगे. वास्तव में ये लोग परोपकारी हैं और इन्हीं के भरोसे संसार चल रहा है. अगर ये न हों ये जो पृथ्वी नाम का ग्रह सूर्य नाम के गैसीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगाना बंद कर दे और दुनिया एक जगह ठहर जाए. तीसरी कटेगरी के दर्शक वे लोग हैं जिन्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं. सिनेमा से भी नहीं. मने परमसंत कटेगरी वाले. इन्हें सिर्फ़ तीन घंटे का मनोरंजन चाहिए होता है और मनोरंजन का मतलब इनके लिए बस मारधाड़, देहदर्शन, नाच-गाने तक सीमित है. इससे ज्यादा कुछ नहीं.
इन तीन वर्गों को भी अब हॉल तक जाने की जरूरत महसूस नहीं होती. क्योंकि नेट 400 रुपये में तीन महीने के लिए उपलब्ध है और लगभग हर हाथ में अच्छा-बुरा किसी न किसी तरह का स्मार्टफोन है. लेकिन फिल्में बनाने वालों का पैसा वसूल तो दर्शक को हॉल में ढटिया कर ही होना है. तो इसके लिए उसे मजबूर किया जाता है. डंडे से हाँक-हाँककर हॉल तक लाया और फिर दो-तीन घंटे के लिए ढटियाया जाता है.
यह डंडा अदृश्य किस्म का होता है. बिना मुद्दे के मुद्दे यानी किसी न किसी कृत्रिम मुद्दे पर बनने वाली फिल्मों पर कृत्रिम विवाद उठाया जाता है. यह कृत्रिम विवाद उठाने के लिए शुरू में कुछ लोगों को पैसा दिया जाता है. बाद में लोग इसमें लोग अपने-आप ही शामिल होते चले जाते हैं. चूँकि देश आजकल राजनीतिक रूप से दो कटेगरी में बँटा हुआ है और दोनों कटेगरियां अपनी पीढ़ियों की वास्तविक दोस्ती तक भुला कर नई-नई बनी छद्म राजनीतिक दुश्मनी निभा रही हैं, तो किसी विवाद में शामिल करने के लिए लोग ढूँढने भी नहीं पड़ते. अधिकतर तो पहले से ही मुफ्त का बेल्ट लगाकर बैठे होते हैं.
याद करिए वो फिल्म जिस पर पूरा राजस्थान धधक उठा था. बाद में रिलीज होने पर इस हाथी के दिल को चीरा तो पता चला कि इक कतर-ए-खूँ भी न निकला. उसके बाद उसी राजपूती आन-बान को बट्टा लगाने वाली बहुत बातें असली दुनिया में हुईं. उसी राजस्थान में ही. लेकिन कुछ हुआ क्या? फिर पता चला क्या किसी सेना का? फिर ये सेना एक टुच्ची फिल्म के लिए कहाँ से टपक पड़ी थी?
ये तो बस हाल का एक विवाद है. ऐसे कम से कम एक हज़ार विवाद भारत में हो चुके हैं. क्या इनसे कभी कोई हल निकला है. आजकल फिर ऐसे ही कुछ प्यालियों में तूफान उठाए जाने की कोशिश की जा रही है. धीरे-धीरे टेम्पो बन भी रहा है और फिर उफन कर बैठ भी जा रहा है. लेकिन होगा क्या? फिर वही ढाक के तीन पात. क्योंकि पहले भी मुद्दे और विवाद दोनों कृत्रिम थे और आज भी स्थिति वही है.
आप याद करिए, सीधे आपके असली मुद्दे को केंद्र में रखकर कोई सच्ची फिल्म बनी हो? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो तीन घंटे में पोएटिक जस्टिस थमा के आपको हॉल से बाहर कर देती हैं. तीन मिनट में साहूकार खेत को हड़पता है और पाँचवें मिनट में शेखचिल्ली टाइप हीरो उसके सारे गुंडों को मारकर गाँव वालों को जिता देता है. किसी राज्य के मुख्यमंत्री को एक दरोगा लतियाते हुए लॉकअप में बंद कर देता है. देखते-देखते फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है और उसके तुरंत बाद पूँजीपति मान जाता है. हम सब जानते हैं कि यह सब सिर्फ हिंदी सिनेमा में होता है, बाकी किसी सिनेमा में भी नहीं. और वास्तविक जीवन से तो इसका उतना भी संबंध नहीं है जितना बुद्धिजीवियों का सच्चाई से होता है.
याद करिए, इतने दिनों में एक भी फिल्म बनी हो भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्या को जमीनी तौर पर संबोधित करती हो? एक भी फिल्म बनी हो जो भारत में शिक्षा-व्यवस्था की बुनियादी समस्याओं को संबोधित करती हो? रोजगार की ही बात उठा लीजिए. अच्छा आइए, इतिहास की ही बात उठा लेते हैं. बाजीराव जैसे योद्धा को हिंदी सिनेमा देवदास बना के धर देता है. विभाजन के नाम पर केवल झूठ का प्रदर्शन है. सौ प्रतिशत शुद्ध झूठ. लिखित और सर्वस्वीकृत ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत. वह भी तब जबकि फिल्में बनाने वाले कुछ बड़े घराने खुद विभाजन के शिकार रहे हैंं. जिस समय विभाजन हुआ, केवल पंजाब ही नहीं बँटा था, बंगाल का सेना चीरा गया था. बंगाल के विभाजन का दर्द कहीं दिखाई देता है क्या? या विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बंग्लादेश) से जो लोग भगाए गए, वे बड़े मजे-मजे में चले आए?
दलित बड़ा प्रिय विषय है हमारे बुद्धिजीवियों का और सिनेमा में बुद्धिजीवी होने के भ्रम के शिकार कम लोग नहीं हैं. मने सब जगह हो सकते हैं बुद्धिजीवी तो सिनेमा में क्यों नहीं? तो दलितों पर उन्होंने खूब बनाया. लेकिन बनाया क्या? उसके दुख की पैरोडी, मजाक. भारत-विभाजन के समय एक जोगेंद्र नाथ मंडल हुआ करते थे. डॉ. अंबेडकर के बाद दूसरे बड़े दलित नेता. दोनों में फर्क यह था कि अंबेडकर वाकई दलित हितैषी थे और सच्चे अर्थों में मनुष्यतावादी भी, मंडलजी के लिए दलित अपने राजनीतिक स्वार्थसाधन का एक उपयोगी सामान मात्र था. तो मंडल जी अपने समय के पाकिस्तान में मंत्री बना दिए गए थे. उन्होंने पाकिस्तान बनवाने के लिए भी दलितों का कुछ इस्तेमाल किया और डॉ. अंबेडकर के मना करने के बावजूद बड़ी मात्रा में दलितों को पाकिस्तान में थोड़े दिन रोका. बाद में जब उन पर इस्लामी कहर बरपना शुरू हुआ तो मंडल जी रह पाए और न दलित. मंडल जी तो खैर बड़े आदमी थे, भाग आए. लेकिन जो आम दलित वहाँ रह गए थे, वे? उनकी सुहि लेने की जहमत न साहित्य ने उठाई और न सिनेमा ने.
सिनेमा की मानें तो थाने में कहीं घूस नहीं चलता. दरोगा जी संसार के सबसे ईमानदार प्राणी हैं. कानून अंधा है, लेकिन जज साहब भगवान से भी सच्चे हैं. झुग्गियाँ उजाड़ी जाती हैं. उजाड़ने वाले पूँजीपति के गुंडे होते हैं. लेकिन झुग्गियां बसाने के लिए हर साल इंसानों की ये जो बाढ़ आती है, ये आती कहाँ से है? यह सब पोएटिक जस्टिस का सतही तौर निपटे जा सकते लायक विषय नहीं हैं. ये और ऐसे ही और कई विषय हमारे सामाजिक जीवन के जटिल यथार्थ हैं. इनमें मसाला नहीं है. कड़वाहट है और जटिलताएँ हैं. और जहाँ यह सब है, वहाँ कम से कम हिंदी सिनेमा तो नहीं जाता.
फिर भी आप हॉल तक जाना चाहते हैं तो जरूर जाएँ. आख़िर जेब आपकी है, समय आपका, मन आपका और ईश्वर की कृपा से झेलने की कूवत भी आपकी ही.




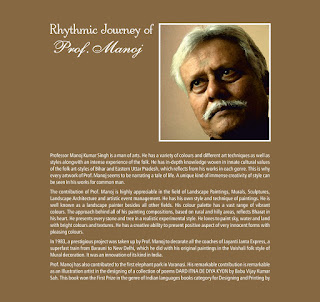


Comments
Post a Comment
सुस्वागतम!!