जहां वृक्ष ही देवता हैं
हरिशंकर राढ़ी
जब हमारा ऑटोरिक्शा जोधपुर शहर से बाहर निकला तो हमें कतई एहसास नहीं था कि जहां हम जा रहे हैं वह स्थान पर्यावरण का इकलौता तीर्थ होने की योग्यता रखता है। सदियों पहले जब पर्यावरण संरक्षण के नाम पर न कोई आंदोलन था और न कोई कार्यक्रम, तब वृक्षों के संरक्षण के लिए सैकडो़ं अनगढ़ और अनपढ़ लोगों ने यहां आत्मबलिदान कर दिया था। आत्माहुति का ऐसा केंद्र किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं हो सकता। लेकिन विडम्बना यह है कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर इतनी चिल्ल-पों मचने और पर्यटन के धुंआधार विकास के बावजूद यह स्थल अपनी दुर्दशा पर रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। इसे तो स्वप्न भी नहीं आता होगा कि देश के पर्यटन मानचित्र में कभी इसका नाम भी आएगा !
राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जोधपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति के अंचल में बसा खेजड़ली गांव किसी भी पर्यावरण प्रेमी के लिए विषेश महत्त्व का हो सकता है। घुमक्कड़ी के क्रम में जब जोधपुर यात्रा का कार्यक्रम बना तो निश्चित हुआ कि खेजड़ली गांव हर हाल में देखना है। मैं उनसे सहमत था। राजस्थान को विषेशतः किलों और महलों का प्रदेश के रूप में जाना जाता है और जो भी वहां जाता है, इनसे बाहर नहीं निकल पाता। हमने सोचा कि इस बार उस भूमि को प्रणाम करके आना है जहां आज से लगभग ढाई सौ वर्ष पहले इस प्रकार की चेतना पैदा हो चुकी थी कि ‘‘सिर साटैं रूख रहे तो भी सस्तो जांण’’ अर्थात् यदि शी देकर भी वृक्षों की रक्षा हो सके तो उसे सस्ता जानो।
यह भी कम हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि पर्यावरण रक्षा के नाम पर हम जिस चिपको आंदोलन की सराहना करते नहीं थकते और जिसका श्रेय हम आज के जिन पर्यावरणविदों को देते हैं, वे उसके अधिकारी नहीं हैं। वृक्षों के संरक्षण का महत्त्व तो यहां तब से दिया जा रहा है जब पर्यावरण प्रदूषण नामक समस्या का जन्म ही नहीं हुआ था। वन संरक्षण की शिक्षा तो इस देश की अनपढ़, अनगढ़ जनता और जनजातियां देती रही हैं। शायद हमारे भी मन में यह भ्रम रह जाता कि चिपको आंदोलन तो उन्नीसवीं सदी की देन है, यदि हम खेजड़ली की यात्रा पर नहीं जाते और बिश्नोइयो का वह त्याग न देखते।
चैदह अगस्त का दिन था। आसमान में बादल छाए हुए थे और रह-रहकर फुहारें आ रही थीं। राजस्थान में बादलों की उपस्थिति और फुहारों का पड़ना कुछ अलग ही आनंददायक होता है। रेलवे स्टेशन के पास अपने होटल से निकलकर जब हमने ऑटोरिक्शा वालों से खेजड़ली चलने की बात की ऐसा नहीं लगा कि वे वहां जाने के अभ्यस्त हैं और प्रायः जाया करते होंगे। कइयों ने अनभिज्ञता प्रकट की तो कुछ ने हमसे ही जानना चाहा कि क्या उसी खेजड़ली चलना है जहां लड़ाई हुई थी? ले-देकर एक ऑटो वाला जानकार निकला जो साढ़े तीन सौ रुपए में आने-जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुल मिलाकर उसे भी पूरी तरह यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हम लोग वहां मात्र घूमने और शहीद स्थल देखने जा रहे हैं।
इस बार जोधपुर में कुछ बारिश हुई थी और इसके प्रमाण में दूर-दूर तक हरियाली फैली थी। मुख्य मार्ग छूट चुका था और अब हम हर सामान्य भारतीय गांव की ओर जाने वाली टूटी-फूटी एकल सड़क पर चले जा रहे थे। कुछ ही दूर गए होंगे कि घास के मैदान में मृगशावकों का झुंड देखकर मन उछल पड़ा। ऐसा नहीं था कि हम पहली बार हिरन देख रहे थे। हां, प्रकृति की गोद में इस तरह उन्मुक्त विचरण करते हुए मृगसमूह देखने का यह पहला अनुभव था। ये मासूम चार पैरों के हिंसक पशुओं से बच भी जाएं, मगर इन्हें दो पैरों के हिंसक समाज से कौन बचाए? यही कारण है कि मानव समाज की अपेक्षा जंगलों में स्वयं को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन याद आया कि यह इलाका कुछ अलग किस्म के लोगों का है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक हिरन के शिकार के अपराध में फिल्म जगत की एक मशहूर हस्ती को भी दंड दिलाने में कोई रियायत नहीं बरती थी। ऐसे लोगों के बीच हिरन स्वच्छंद क्यों न विचरें?
खेजड़ली गांव के शहीद स्मारक से ऑटो ड्राइवर भी पूरी तरह परिचित नहीं था। गांव में एक-दो लोगों से पूछकर वह शहीद स्मारक के सामने ऑटो लगा दिया। कुछ छिटपुट ग्रामीण इधर-उधर घूम रहे थे। सामने चारदीवारी से घिरा एक बेतरतीब सा बाग नजर आ रहा था। एक सामान्य से गेट को पारकर हम तीनों लोग अंदर घुसे तो हमारा स्वागत रास्ते के दोनों ओर घूम रहे मोरों ने किया। बारिश का मौसम था ही और मोर भी अपने पूरे रवानी में थे। रह-रहकर उनकी कुहुक रोमांचित कर जाती थी और इस प्रारंभिक स्वागत से ही मन बाग-बाग हो उठा। अभी दो-चार कदम ही चले होंगे कि घुटनों तक धोती और बनियान पहने एक देहाती से सज्जन हमारी ओर बढ़े। बड़े ही सलीके से हाथ जोड़कर उन्होंने हमें नमस्ते किया और परिचय पूछा। हम उनके राजस्थानी शिष्टाचार और सादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वैसे भी गांव में पले-बढ़े हम तीनों यात्री माटी की खुशबू को खूब पहचानने वाले थे। ये सज्जन थे शहीद स्थल के कर्मचारी वेराराम जी। हमारा परिचय पाकर और विषेशतः यह जानकर कि हम खेजड़ली के इतिहास और बलिदान स्थल को प्रणाम करने आए हैं, बहुत खुश हुए।
जब हमारा ऑटोरिक्शा जोधपुर शहर से बाहर निकला तो हमें कतई एहसास नहीं था कि जहां हम जा रहे हैं वह स्थान पर्यावरण का इकलौता तीर्थ होने की योग्यता रखता है। सदियों पहले जब पर्यावरण संरक्षण के नाम पर न कोई आंदोलन था और न कोई कार्यक्रम, तब वृक्षों के संरक्षण के लिए सैकडो़ं अनगढ़ और अनपढ़ लोगों ने यहां आत्मबलिदान कर दिया था। आत्माहुति का ऐसा केंद्र किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं हो सकता। लेकिन विडम्बना यह है कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर इतनी चिल्ल-पों मचने और पर्यटन के धुंआधार विकास के बावजूद यह स्थल अपनी दुर्दशा पर रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। इसे तो स्वप्न भी नहीं आता होगा कि देश के पर्यटन मानचित्र में कभी इसका नाम भी आएगा !
 |
| खेजडली का शहीद स्मारक छाया : हरिशंकर राढ़ी |
यह भी कम हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि पर्यावरण रक्षा के नाम पर हम जिस चिपको आंदोलन की सराहना करते नहीं थकते और जिसका श्रेय हम आज के जिन पर्यावरणविदों को देते हैं, वे उसके अधिकारी नहीं हैं। वृक्षों के संरक्षण का महत्त्व तो यहां तब से दिया जा रहा है जब पर्यावरण प्रदूषण नामक समस्या का जन्म ही नहीं हुआ था। वन संरक्षण की शिक्षा तो इस देश की अनपढ़, अनगढ़ जनता और जनजातियां देती रही हैं। शायद हमारे भी मन में यह भ्रम रह जाता कि चिपको आंदोलन तो उन्नीसवीं सदी की देन है, यदि हम खेजड़ली की यात्रा पर नहीं जाते और बिश्नोइयो का वह त्याग न देखते।
चैदह अगस्त का दिन था। आसमान में बादल छाए हुए थे और रह-रहकर फुहारें आ रही थीं। राजस्थान में बादलों की उपस्थिति और फुहारों का पड़ना कुछ अलग ही आनंददायक होता है। रेलवे स्टेशन के पास अपने होटल से निकलकर जब हमने ऑटोरिक्शा वालों से खेजड़ली चलने की बात की ऐसा नहीं लगा कि वे वहां जाने के अभ्यस्त हैं और प्रायः जाया करते होंगे। कइयों ने अनभिज्ञता प्रकट की तो कुछ ने हमसे ही जानना चाहा कि क्या उसी खेजड़ली चलना है जहां लड़ाई हुई थी? ले-देकर एक ऑटो वाला जानकार निकला जो साढ़े तीन सौ रुपए में आने-जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुल मिलाकर उसे भी पूरी तरह यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हम लोग वहां मात्र घूमने और शहीद स्थल देखने जा रहे हैं।
 |
| हरियाली और मृग शावक छाया : हरिशंकर राढ़ी |
मृगशावकों का कलोल देखने से हम भी स्वयंको रोक न सके और ऑटो रुकवाकर उतर पड़े। कैमरा निकाला और दो चार फोटो खींचे। एक झुंड निकलता तो दूसरा आ जाता और खेलते-कूदते उड़ंछू हो जाता छोटे शावक टेढ़े-मेढ़े उछलते हुए अपनी मांओं के चक्कर लगाते और शैतानी करते हुए दूर तक भाग जाते। माताएं परेशान होतीं, शावकों को मजा आता। बीच-बीच में वे दो चार घासें भी चर लेते, लेकिन लगता था कि वे घासें कम, वातावरण का स्वाद ज्यादा ले रहे थे। पेड़ों पर पक्षी कलरव कर रहे थे। पेड़ भी कौन से थे- अधिकांशतः बबूल, कीकर और खेजड़ी के, जिनका अधिकांश जीवन गुरबत में ही बीतता है- पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करते हुए। इस वर्ष कुछ बारिश हो गई थी इसलिए इनकी खुशी का पारावार नहीं था। वह ख़ुशी इनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। इनके भी दिन बहुर आए थे और वही संतुष्टि दिख रही जो गरीब को भरपेट भोजन मिल जाने पर होती है। इनका तो जीवन ही ऐसा है कि भूखे पेट भी दूसरों के लिए संघर्ष करते रहते हैं।
 |
| खेजडली का वृक्ष पकड़े वेराराम जी |
घटना सन् 1730 की है। जोधपुर के तत्कालीन राजा अभय सिंह अपने किले का विस्तार कराना चाहते थे और इसके लिए उन्हें खेजड़ी के वृक्षों की आवश्यकता थी। खेजड़ी के वृक्षों से चूना तैयार किया जाता था। खेजड़ली गांव के आस-पास इन वृक्षों की बहुतायत है और राजा ने अपने मंत्री गिरधर भंडारी को खेजड़ी के तमाम वृक्षों को कटवा लाने का आदेश दिया। जब मंत्री महोदय राजाज्ञा के पालन हेतु दल-बल सहित इसे इलाके में पहुंचे और खेजड़ी वृक्षों को कटवाना शुरू किया तो यह खबर गांवों में जंगल की आग की तरह फैली। गुरु जम्भेश्वर में अटूट आस्था रखने वाले बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होकर विरोध करने लगे। जब मंत्री ने सैन्यबल का प्रयोग किया तो 84 गांवों के बिश्नोई इकट्ठा हो गए और अमृता देवी के नेतृत्व में उन्होंने वृक्षों को अपनी बाहों में भर लिया और किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने नारा दिया कि ‘‘सिर साटैं रूख रहे तो भी सस्तो जांण’’। आत्मबल और सैन्यबल का भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें 363 बिश्नोई मारे गए। खबर जब राजा अभय सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने इस जनांदोलन के सामने झुकने में ही भलाई समझी। यह विश्व का पहला चिपको आंदोलन था जो बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सफल हुआ था। आज खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है।
 |
| क्षेत्रीय बच्चों के साथ लेखक (टोपी लगाए ) और बद्री प्रसाद यादव |
पर्यावरण संरक्षण हेतु आज का सुषिक्षित और जागरूक समाज इतना बड़ा बलिदान षायद ही दे ! वेराराम जी की वर्णन षैली और गाथा की गंभीरता से हम रोमांचित हो चुके थे। उनसे कुछ देर बाद पुनः मिलने का वादा कर हम षहीद स्मारक की ओर चल पड़े। उद्यान परिसर में ही एक कोने में एक छोटा किंतु अच्छा सा स्मारक बना हुआ है। यह भी देखकर सुखद लगता है कि इसकी साफ-सफाई भी अन्य षहीद स्मारकों की तुलना में अधिक है। पूरी घटना को संक्षेप में बयान करता हुआ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो अभी अच्छी हालत में है। स्मारक पर हम भी नतमस्तक हुए। बच्चों का एक समूह वहां घूम रहा था। अपनी अधिकतम जानकारी उन्होंने हमें दी और बताया कि साल में एक बार इस स्मारक पर बड़ा जमावड़ा होता है। वह दिन बलिदान दिवस की बरसी के रूप में मनाया जाता है। स्मारक के पीछे गुरु जम्भेष्वर जी का एक मंदिर निर्माणाधीन था जो बिष्नोइयों की प्रकृति प्रियता और श्रद्धा का प्रतीक है।
पूरा पर्यावरण शहीद स्मारक खेजड़ी के वृक्षों से आच्छादित है जहां भांति-भांति के पक्षी स्वच्छंद भाव से घूमते मिल जाते हैं। वापसी में वेराराम जी से दोबारा बातचीत हुई। हमने यह तलाशने की कोशिष की कि क्या वहां के लोगों में पेडों और जानवरों की सुरक्षा को लेकर वही जज्बा है जो उनके पूर्वजों ने लगभग ढाई सौ साल पहले दिखाया था। उन्होंने बताया कि प्राणों की तुलना में पेड़ों की कीमत तो उनकी परंपरा रही है, वह कैसे अलग हो सकती है!
 |
मन आश्वस्त हुआ कि शायद प्रकृति बची रहे। जब तक हमारी बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण रहेगी और प्रकृति में ईश्वर के वास का ‘अंधविश्वास ’ बचा रहेगा, धरती पर मानव के अतिरिक्त दूसरे जीव और पेड़-पौधे भी जीवित रहेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि प्रकृतिरक्षा के इस तीर्थ को मानो गोपनीय रखा गया है। न तो कोई प्रचार-प्रसार, न तो पाठ्यक्रम में चर्चा और न तो वहां तक पहुंचने की सुविधाएं। जो प्रेरणा नई पीढ़ी को यहां से मिल सकती है, वह शायद ही कहीं से मिले। हम कितने भी वन्य जीव अभयारण्य बना लें, बायो रिजर्व स्थापित करने का दावा कर लें और कितने भी कानून बना लें, विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों को विलुप्त होने से नहीं रोक पांएगे। हमें ऐसे अनेक ‘खेजड़ली’ तलाशने और तराशने होंगे। हमने इसे भोली मानसिकता को प्रणाम किया और वेराराम जी को धन्यवाद देकर जोधपुर वापस चल पड़े।
हमारा अगला प्रोग्राम ऐतिहासिक स्थल मंडोर देखने का था। अपराह्न ढाई बजे हम मंडोर पहुंचे तो मौसम उमस भरा हो चुका था और धूप चुभने लगी थी। अन्य पर्यटक स्थलों की भांति यहां भी रेहड़ी-खोमचे तथा अन्य विक्रेताओं की भीड़ और शोर मौजूद था। मंडोर जोधपुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर की ओर एक छोटी से पहाड़ी नदी नागाद्रि के किनारे बसा हुआ है जो अब नागादड़ी कहलाती है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर था और यह नगर सन् 1459 तक राठौड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। इसी वर्ष राव जोधा जी ने आसपास के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया और नए बसे शहर जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। बहुत दिनों तक मंडोर-जोधपुर राजघराने के दिवंगतों का दाह संस्कार यहीं होता रहा जिससे यहां अनेक शासकों के देवल (स्मारक स्थल) भी मिलते हैं।
(शेष भाग शीघ्र ही … )
 |
| खेजडली उद्यान में नीम के वृक्ष पर बैठे मोर का वास्तविक दृश्य छाया : हरिशंकर राढ़ी |
(यह वृत्तान्त समग्र रूप में दो किश्तों में पोस्ट किया जा रहा है. पहली किश्त में केवल खेजडली और दूसरी में शेष जोधपुर आपके लिए कुछ दिनों बाद। )




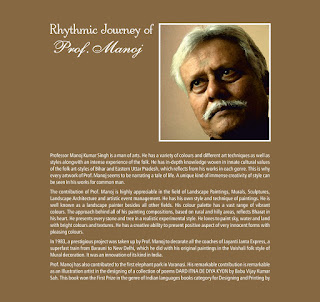


सारे दृश्य ख़ुद-ब-ख़ुद तरोताज़ा हो गए.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteराजस्थान में जल का मान है, पर्यावरण का मान है। चिपको आन्दोलनों की प्रेरणा काश हर जगह फैलती तो पर्यावरण सिसक नहीं रहा होता।
ReplyDeleteअपनी भाषा में किसी भी विषय के प्रश्न के उत्तर, विषय-आधारित वृक्षारोपण के लिए संपर्क: ०९४२५६०५४३२ सुमित
ReplyDeleteजानकारी से भरपूर रोचक आलेख के लिए धन्यवाद। धरती हरी -भरी रहे यह जीवन के लिए जरुरी है। विश्नोई समुदाय का इस दिशा में त्याग और योगदान सराहनीय है।
ReplyDeleteA11275B071
ReplyDeleteeski mmorpg oyunlar
sms onay
turkcell mobil bozum
güvenilir takipçi satın alma
takipçi fiyatları