अजंता: जहां पत्थरों में अध्यात्म है
-हरिशंकर राढ़ी
 |
| बस में अजंता की ओर : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
एलोरा तो देख आए किंतु अजंता का आकर्षण एलोरा से भी बड़ा था। कारण जो भी रहा हो, चाहे वह अजंता - एलोरा के युग्म में पहले आता है, इसलिए या फिर अब तक की पढ़ाई लिखाई और इंटरनेट से एकत्र की गई जानकारी के कारण। जलगांव में रात अच्छी गुजरी थी और नींद तो खूब आई ही थी। सुबह की चाय के बाद नाश्ता और दो बार चाय लेने के बाद मन में उत्साह थोड़ा और बढ़ गया। लगभग दस बजे हम जलगांव से अजंता की गुफाओं के लिए कूच कर गए। बैग - सैग गाड़ी में ही जमा लिया क्योंकि वापसी हमें भुसावल से करनी थी। जलगांव से अजंता गुफाओं की दूरी 62 किलोमीटर है और भारतीय राजमार्ग की परंपरा के अनुसार तेज चलने पर भी लगभग डेढ़ घंटा लग ही जाता है। हम लोग तो वैसे भी तसल्ली से चलने रास्ते का आनंद लेने वाले पथिक हैं, सो डेढ़ घंटे से कुछ ज्यादा ही समय खर्च कर अजंता गुफाओं तक पहुंच गए।
विश्व धरोहर अजंता
 |
| गुफा परिसर में प्रवेश के बाद : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया है, सो इसका प्रभाव वहां के वातावरण पर पड़ना ही है। मजबूरी में ही सही, नियमों का पालन करना है, साफ-सफाई दिखानी ही है, सो यह सब अंतर साफ दिखा। अपनी अर्वाचीन भारतीय संस्कृति का जो जादू - रेहड़ी, खोमचा, भुट्टा वगैरह का अतिक्रमणीय दृष्य अपने पर्यटन स्थलों पर देखने को अनिवार्य रूप से देखने को मिल जाता है, वह यहां नहीं था। उसका परिणाम यह होता है कि एक आम भारतीय दर्शक को लगता है कि किसी महत्त्वहीन जगह पर आ गया है। परंतु हम कर भी क्या सकते हैं, भारतीय नियमों को मानें या न मानें, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। और फिर जिसे यूनेस्को ने गोद ले रखा हो, उसे हम आंखें तरेर भी कैसे सकते हैं ?
 |
| दीवारों पर गज़ब के मिथुन : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
चलिए, एक सुखद एहसास हुआ कि हम हल्ला-गुल्ला और शोर -शराबे से बच गए। जिस पर्वतीय हिस्से में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, उसके पद तक ही सामान्य वाहनों को जाने की अनुमति है। गाडि़यों वहीं पार्क करने की सुविधा है। वहां से आगे पुरातत्व विभाग की देख-रेख में प्रदूषण रहित मिनी बसें प्रशासन की ओर से चलाई जाती हैं और हर पर्यटक को उन्हीं बसों में बैठकर गुफा तक जाना होता है। हाँ, ये बसें निश्शुल्क नहीं हैं परंतु किराया तार्किक है। ऐसी ही एक बस में हम तेरह जने सवार हुए और सर्पाकार मार्ग का आनंद लेते हुए गुफा के प्रवेशद्वार तक पहुंच लिए। यहां टिकट लेकर हम भी निर्देशित दिशा में गुफा की ओर चल पड़े।
अभी अप्रैल की शुरुआत ही थी और लगभग ग्यारह बजे होंगे किंतु धूप उस सूखी पहाड़ी में खलनायिका की तरह हमें तंग कर रही थी। वैसे भी यह प्रदेश कर्क रेखा क्षेत्र में पड़ता है और सूर्य उत्तरायण की स्थिति में कर्क से संक्रांति करने वाला था। (अजंता की भौगोलिक स्थिति 20°31अक्षांश उत्तर है जो कर्क रेखा - 230 उत्तर से बहुत निकट है) इस बात को मैं समझ रहा था किंतु समझने से धूप कम नहीं हो जाती। ऊपर से अंदर किसी भी प्रकार के खान-पान की व्यवस्था नहीं क्योंकि विश्व धरोहर के क्षतिग्रस्त होने का खतरा। सो, हम अपने साथ ले मौजूद पानी की एक बोतल पर निर्भर थे। गर्मी के कारण आस-पास के पेड़-पौधे और झाडि़यां सूख रही थीं। लेकिन मन में खुशी थी कि आज हम उस स्थान तक आ ही गए जो विश्व विरासत घोषित हो चुका है। आखिर क्या रहा होगा उन लोगों के मन में जिन्होंने इस प्रकार के गैर व्यावसायिक कार्य में इतना पैसा लगाया ? यह प्रश्न मेरी मानसिकता की उपज नहीं था अपितु उस विचारधारा के विरुद्ध था जिसमें समाज का एक वर्ग केवल आर्थिक प्रगति को ही मानव का विकास मानता है; केवल उसे ही सार्थक कार्य मानता है जिससे उसकी मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त भोग - विलास की सामग्री पैदा हो सके। उसकी नजर में कला, साहित्य और शिल्प सिवाय चोंचलेबाजी के कुछ नहीं है। इस बात से असहमत नहीं हुआ जा सकता है कि मानवता यह है कि हर मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होनी ही चाहिए और हमारा प्रथम प्रयास भी इस दिशा में होना चाहिए। किंतु केवल मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में इतना व्यस्त हो जाए कि वह अपनी मानसिक भूख की चिंता ही न करे और अपनी सभ्यता के आयाम ही छोड़ दे, यह भी न्याय नहीं होगा। मुझे याद आया कि औद्योगीकरण के युग में योरोप में एक समय ऐसा आया था जब कविता और साहित्य की प्रासंगिकता पर आक्षेप लगने शुरू हो गए थे। तब साहित्य की प्रतिरक्षा में फिलिप सिडनी ने ‘एन अपोलोजी फाॅर पोएजी’ लिखकर निहायत भौतिकवादियों को जवाब दिया था। आज फिलिप सिडनी का वह लेख मील के पत्थर के रूप में याद किया जाता है।
 |
| विहंगम दृश्य : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
गुफाओं की खोज
 |
| ये गुफा महल ! : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
यद्यपि आज यह स्वीकार किया जा चुका है कि गुफाओं का निर्माण 200 ई0पू0 शुरू हुआ था और अनेक कालों से गुजरता हुआ यह छठी शताव्दी तक पूरा हुआ था, किंतु इसकी खोज 1819 में संयोगवश हो गई थी। मद्रास प्रेसीडेंसी का अफसर जाॅन स्मिथ यहां शेर के शि कार की तलाश में अचानक ही पहुंच गया था। जब वह गुफा नंबर 10 के सामने पहुंचा तो स्थानीय लोग गुफा का प्रयोग प्रार्थना स्थल के रूप में कर रहे थे और वहां आग जल रही थी। दरअसल ये गुफाएं पर्वत के अंदरूनी हिस्से में बनी हुई हैं। चारो तरफ ऊंची पहाडि़यां, पेड़-पौधे और घनी झाडि़यां थीं जिनके अंदर यह कहीं एक रहस्य की भांति समा गई थी। जाॅन स्मिथ गुफाओं को देखकर हैरान हो गया और उसके लौटने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सुध लेना शुरू किया और अजंता की गुफाएं आज विश्व धरोहर में शीर्षस्थ रूप से स्थापित हो चुकी हैं।
गुफाओं का स्थापत्य और सौंदर्य
 |
| देवताओं की मूर्तियां : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
एलोरा की गुफाओं की भांति अजंता की गुफाओं को क्रमांकित किया गया है। गुफाओं की कुल संख्या 29 है और जैसे -जैसे आगे बढ़ते हैं, गुफाओं का सौंदर्य बढ़ता सा प्रतीत होता है। इन गुफाओं को संभवतः कालक्रम के अनुसार निर्मित किया गया और उसी के अनुसार इन्हें बांटा भी जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुफा क्रमांक 9, 10, 12, 13 एवं 15 ई0पू0 100 से लेकर 100 ई0 सन् के बीच बनाई गई थीं। इस समय सत्त्वाहन वंश का राज्य था और वे कला के बड़े समर्थक थे। इन गुफाओं में क्रमांक 9,10ए19ए26 तथा 29 चैत्यगृह और शेष विहार हैं। इतिहासकारों द्वारा निर्माणकाल एवं शैली के आधार पर गुफाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कुल छह गुफाओं को उत्खनन बौद्धकाल के हीनयान युग में हुआ। गुफा संख्या 8,10,12, 15 अ, ईसा पूर्व की हैं।
गुफाओं के निर्माण का दूसरा काल ईसा की पांचवीं -छठी शती हैं। इनके उत्कीर्णन का प्रयोजन संभवतः वाकटकों के प्रति सामंतों की निष्ठां का प्रदर्शन था। इसका समर्थन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अजंता गुफाओं के परिसर में लगाया गया शिलालेख भी है। वाकाटक नरेश हरिषेण के मंत्री वराहदेव ने गुफा संख्या 16 का निर्माण कराकर बौद्धसंघ को समर्पित किया। चीनी घुमक्कड़ ह्वेनसांग ने भी गुफाओं का जिक्र किया है जबकि वह यहां नहीं आया था। इस गुफा के संबंध में भारतीय पुरातत्व कहता है कि गुफा संख्या 16 महायान संप्रदाय से संबंधित है। यह एक उत्कृष्ट कृति है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण है। इसके प्रदक्षिणापथ चंवरधारी बोधिसत्त्व एवं मालाधारी गंधर्व आकृतियों से घिरे सिंहासनस्थ बुद्ध का चित्रण है। मरणासन्न राजकुमारी, असित की भविष्यवाणीं , नंद का मनपरिवर्तन, माया का स्वप्न, श्रावस्ती का चमत्कार एवं सुजाता का खीर प्रदान करना प्रमुख चित्र हैं।
 |
| यह भी एक गुफा है ! :छाया - हरिशंकर राढ़ी |
भित्तिचित्र:
अजंता गुफाओं में जहाँ विशाल पहाड़ को काटकर अथक श्रम एवं अजेय धैर्य से सुंदर उत्कीर्णन किया गया है, वहीं भित्तिचित्रों को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ा युग कहलाने वाले उस युग में जिस प्रकार चित्रकारी करके उसे संरक्षित किया, वह किसी भी संवेदनशील मनुष्य को दाँतों तले उँगली दबाने पर मजबूर कर देगा। इसमें संदेह नहीं कि समय के साथ इनका बहुत क्षरण हुआ है, फिर भी विशेषज्ञों की सहायता से इन भित्तिचित्रों को संरक्षित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। इनके स्वास्थ्य को देखते हुए भित्तिचित्रों वाली गुफाओं में फोटोग्राफी निषिद्ध है। हाँ, फ़्लैश चमकाए बिना फोटोग्राफी करते हुए लोग देखे जा सकते हैं, किंतु नीम उजाले में लिए गए फोटो बेकार से ही नजर आते हैं।
 |
| छाया - हरिशंकर राढ़ी |
सभी भित्तिचित्र बौद्धकथाओं को ही आधार बनाकर चित्रित किए गए हैं। स्पष्ट है कि उस समय बौद्ध धर्म के प्रति लोगों के मन में विशेष रुझान रहा होगा। तमाम राजाओं ने रुचि एवं उदारतापूर्वक इन गुफाओं के निर्माण में अकूत धन खर्च किया होगा। अजंता गुफाओं के बड़े -बड़े हाॅलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी चोटों से ये आग्नेय शैलें कटी होंगी और छेनी हथौड़ी की हर चोट पर कितना धन खर्च हुआ होगा। ईश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि ये गुफाएँ धर्मांधता की भेंट नहीं चढ़ीं, हालांकि उसके पीछे इनकी दुर्गमता और अज्ञात होना अधिक महत्त्वपूर्ण कारक है।
वाल्टर एम स्पिंक का शोध :
मिशिगन विश्वविद्यालय में एशियाई कला एवं इतिहास (Asian Art and History ) के प्रोफेसर वाल्टर एम स्पिंक ने अजंता पर गहन एवं आधिकारिक शोध किया और आज हम उन्हीं के शोध के बल पर अजंता गुफाओं के बारे में कुछ कह पाते हैं। हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्व विद्यालय के इस विद्वान ने भारत सरकार के अनुरोध पर अजंता, एलोरा और एलीफैंटा गुफाओं पर गहन शोध किया। सन् 2010 तक इनकी पुस्तक अजंता: हिस्ट्री एंड डिवैलपमेंट (Ajanta : History and Development ) के पांच खंड आ चुके हैं। स्पिंक ने उत्कीर्णन एवं कला की शैली जैसे साक्ष्यों के आधार पर संक्षिप्त विधि से पूरी जानकार दी है और अजंता के निर्माण को तिथिवार विभाजित किया है।
 |
| घोड़े की नाल का नज़री नक्शा : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
दूर से देखने पर गुफाएँ घोड़े की नाल के आकार की नजर आती हैं। अंततः हम भी इन्हें देखते - समझते दूसरे सिरे पर जा पहुँचे और थककर बैठ गए। अन्य पर्यटकों को देखने समझने का भी एक अलग मजा होता है। सबके अपने दृष्टिकोण होते हैं और अपने मूल्यांकन। कुछ देर विश्राम करके हमने वापसी का मन बनाया।
 |
| पहाड़ी को काट कर बना स्तम्भ : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
मोलभाव वाला भोजनालय:
गुफाओं से बाहर निकले तो भूख का तीव्र एहसास हुआ। प्रवेशद्वार से अंदर पहुंच जाने के बाद तो खाने की कोई सामग्री मिलती नहीं, अतः लौटते-लौटते भूख भयंकर होने लग जाती है। प्रवेशद्वार के पास ही एक रेस्टोरेंट था, सो हम भी उधर ही खिंचे चले गए। दोपहर हो गई थी, अतः भोजन कर लेने में ही भलाई थी। परंतु, रेस्टोरेंट में प्रवेश करने पर एक विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा, जैसा कभी किया ही नहीं था। वहाँ कोई स्थिर मूल्यसूची हमें देखने को नहीं मिली। पर्यटन का अनुभव हमें यही बताता है कि ऐसी जगहों पर रेट मालूम करके ही खाना पीना चाहिए, क्योंकि खाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका भाव पसंद न आने पर आप वापस कर सकें । फिर या तो गला दबाकर भुगतान करिए या फिर लड़ाई। यहाँ रेस्टोरेंट का माहौल न जाने क्यों संतोषजनक सा नहीं लग रहा था। सो हमने आॅर्डर देने से पहले रेट मालूम किया। उसने प्रति थाली 150 रुपये बताया। अन्य ग्राहक भी भोजन कर रहे थे और थाली की शक्ल देखकर वह भोजन आधी से कम कीमत का लग रहा था। सो हमने वहां से निकल जाने में भलाई समझी। कुल मिलाकर हम तेरह जने थे, सो मालिक ने अपने एक कारिंदे को हमारे पीछे लगाया। फुटपाथी दलाल की तरह उसने अपनी उसी थाली का रेट घटाना शुरू किया और लगभग सौ मीटर तक पीछा करते-करते 40 रुपये तक आ गया। भोजन के मामले में ऐसी बार्गेनिंग हमने आज तक नहीं देखी थी। इस पर मुझे बहुत चिढ़ आती है और वहां भी आ रही थी। इष्टदेव जी भी गुस्से वाले मोड में आ गए थे। अंततः उसे डांटते हुए यह कहकर वापस भेजा गया कि तुम मुफ्त में खिलाओ तो भी हम तुम्हारे यहां नहीं खाने वाले!
और भूख को जज़्ब करके हम प्रदूषणरहित बस में बैठे। पार्किंग में अपनी गाड़ी पकड़ी और भोजन रास्ते में करने का निश्चय करके (और हमने रास्ते में ठीक से भोजन किया) भुसावल जंक्शन के लिए रवाना हो गए। वहाँ से अपनी ट्रेन जो थी दिल्ली के लिए !
 |
| अंतिम गुफा के पास बैठे बच्चे : छाया - हरिशंकर राढ़ी |
उपयोगी जानकारियाँ:
अजंता किसी भी ट्रेन रूट पर सीधे नहीं पड़ता। दिल्ली मुंबई रूट (वाया भुसावल) पर जलगाँव या भुसावल उतरकर रोडवेज बस या टैक्सी से अजंता गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। टैक्सी कर लेना बेहतर होता है। जलगाँव स्टेशन से अजंता की दूरी 52 किलोमीटर और भुसावल जंक्शन से 62 किमी है। औरंगाबाद से यह दूरी 100 किमी है। पूरे महाराष्ट्र में बस सेवा अच्छी है।
कब जाएँ:
अजंता की भौगोलिक स्थिति कर्क रेखा के आस-पास है अतः यहां
गर्मी ज्यादा पड़ती है। सर्वाधिक उपयुक्त मौसम अक्टूबर से मार्च तक का होता है।
दर्शन समय: साप्ताहिक दिनों में प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक, सोमवार बंद।





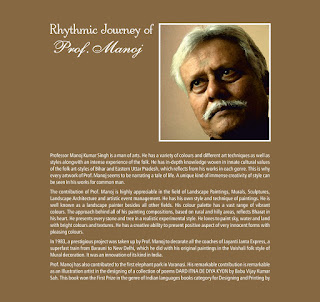



बढ़िया जानकारीपरक लेख....
ReplyDeleteबेहतरीन जानकारी। इसी तरह ब्लाग पर संजीदा लेखन करते रहें। फेसबुक ट्विटर तो बास चलताऊ हैं।
ReplyDeleteDhanyavaad Monika ji and Tripathi ji for your comments.
ReplyDeleteआपका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका ब्लॉग मेरे ब्लॉग "नवीन जोशी समग्र" के हिंदी ब्लॉगिंग को समर्पित पेज "हिंदी समग्र" (http://navinjoshi.in/hindi-samagra/) में शामिल किया गया है। अन्य हिंदी ब्लॉगर भी अपने ब्लॉग को यहाँ चेक कर सकते हैं, और न होने पर कॉमेंट्स के जरिये अपने ब्लॉग के नाम व URL सहित सूचित कर सकते हैं।
ReplyDeleteThanks Joshi ji for your comment and inclusion of this blog.
Delete85DB91A708
ReplyDeletekiralık hacker
hacker arıyorum
belek
kadriye
serik
331B9D8618
ReplyDeletehacker arıyorum
hacker kirala
tütün dünyası
hacker bulma
hacker kirala